स्वामी विवेकानंद व्यक्तित्व पर एक संक्षिप्त लेखनी | स्वामी विवेकानंद एक दार्शनिक की नजर से
Swami Vivekanand Philosophical Thought | My view’s Swami Vivekanand | Swami Vivekanand
“” आदरणीय शिरोमणि स्वामी विवेकानंद एक दार्शनिक की नजर से “”
स्वामी विवेकानंद एक अद्वितीय संत, कर्मयोगी, और युगद्रष्टा थे, जिनके व्यक्तित्व में भारतीय आध्यात्मिकता की गहराई, विद्वता की ऊंचाई, और सेवा भावना की व्यापकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उनका जीवन भारतीय संस्कृति, वेदांत दर्शन और मानवीय मूल्यों का सजीव प्रतीक था। वे न केवल धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं के प्रचारक थे, बल्कि उन्होंने समाज को कर्मयोग, आत्मनिर्भरता और सह-अस्तित्व का मार्ग दिखाया। उनका व्यक्तित्व ओजस्वी वाणी, असीम करुणा, और अनवरत कार्यशीलता का आदर्श रूप में प्रलक्षित होता है।
स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण मात्र भारत तक सीमित नहीं था; वे मानवता के उत्थान के लिए समर्पित थे। उनका संदेश, जो आत्म-जागृति, सेवा, और सार्वभौमिक एकता पर आधारित था, आज भी प्रेरणा का अमूल्य स्रोत है। स्वामी विवेकानंद का प्रभाव भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को वैश्विक पहचान दिलाने में अद्वितीय रहा। उनके द्वारा 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में दिया गया भाषण न केवल ऐतिहासिक था, बल्कि इसने पूरी दुनिया को भारतीय वेदांत और योग के गहन संदेश से परिचित कराया। उनके शब्द
“मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों” ने धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के प्रति भाईचारे का संदेश दिया। उनका विचार था कि धर्म केवल उपदेश का विषय नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। “उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत” जैसे उनके प्रेरक वाक्य उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और कर्मशीलता को दर्शाते हैं।
मानस द्वारा उनके विशाल व्यक्तित्व की छवि में अमूल्य विचारों को दार्शनिक दृष्टि से रखने का प्रयास निम्न बिंदुओं के तहत किया है।
- अद्वैत वेदान्त का दर्शन –
अद्वैत वेदान्त, जिसे आदि शंकराचार्य ने प्रमुख रूप से प्रचारित किया, यह कहता है कि ब्रह्म (परम सत्य) और आत्मा एक हैं। स्वामी विवेकानंद ने इस सिद्धांत को अपने जीवन-दर्शन और शिक्षाओं का आधार बनाया।
प्रासंगिक श्लोक:
“सर्वं खल्विदं ब्रह्म”
[ छांदोग्य उपनिषद (3.14.1) ]
भावार्थ :
“यह सब (जो कुछ भी है) वास्तव में ब्रह्म है।” यानि “ यह पूरा विश्व ही ब्रह्म है।”
“” यह सम्पूर्ण संसार ही ब्रह्म है। प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु में ब्रह्म का वास है। “”
अन्य प्रासंगिक श्लोक :
“अहम् ब्रह्मास्मि।”
[ बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 ]
भावार्थ :
- “अहम्” = मैं
- “ब्रह्म” = ब्रह्म, यानी परम सत्य, परमात्मा या सर्वोच्च सत्ता
- “अस्मि” = हूं
इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है: “मैं ब्रह्म हूं।”
यह आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत (अभेद) को व्यक्त करता है, जो अद्वैत वेदान्त का मुख्य सिद्धांत है।
स्वामी विवेकानंद ने “अहम् ब्रह्मास्मि” के संदेश को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। उनके विचार में –
- प्रत्येक व्यक्ति दिव्य है –
- हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्यता है, जो ब्रह्म से ही आई है।
- आत्म-ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है।
- आत्म-विश्वास का संदेश –
- “तुम कमजोर नहीं हो, तुम अनंत हो।”
- विवेकानंद ने कहा कि इस वाक्य का उद्देश्य आत्मा को उसकी असीम शक्ति का बोध कराना है।
- मानवता का उत्थान –
- जब व्यक्ति “मैं ब्रह्म हूं” की अनुभूति करता है, तो वह स्वयं को दूसरों से अलग नहीं देखता।
- इससे प्रेम, सेवा और समानता का भाव विकसित होता है।
संदर्भ और अन्य महावाक्य –
“अहम् ब्रह्मास्मि” चार महावाक्यों (उपनिषदों के प्रमुख वाक्यों) में से एक है:
- “प्रज्ञनम् ब्रह्म।” [ ज्ञान ही ब्रह्म है। – ऐतरेय उपनिषद ]
- “अहम् ब्रह्मास्मि।” [ मैं ब्रह्म हूं। – बृहदारण्यक उपनिषद ]
- “तत्त्वमसि।” [ तुम वही हो। – छांदोग्य उपनिषद ]
- “अयम् आत्मा ब्रह्म।” [ यह आत्मा ही ब्रह्म है। – माण्डूक्य उपनिषद ]
इन महावाक्यों का उद्देश्य आत्मा और ब्रह्म की एकता को समझाना है।
अन्य प्रासंगिक श्लोक :
“ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति।”
[ मुण्डकोपनिषद (2.2.11) ]
“” जो ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म बन जाता है। “”
स्वामी विवेकानंद ने इसे मानवता के उत्थान का आधार बनाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दिव्यता है और उसे पहचानना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है।
इन्ही आधारों पर “मानव सेवा ही भगवान की सेवा” का संदेश दिया।
वे कहते थे– “दरिद्र नारायण” की सेवा करो, क्योंकि प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति में भगवान का वास है।
- आत्मा की अमरता और स्वाधीनता –
वेदान्त का यह सिद्धांत कि आत्मा अमर और शाश्वत है, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का मुख्य आधार था। उन्होंने आत्म-ज्ञान और स्वाधीनता को जीवन का परम उद्देश्य बताया।
प्रासंगिक श्लोक :
“” न जायते म्रियते वा कदाचि
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे।“”
[ भगवद गीता 2.20 ]
भावार्थ :
आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु। वह अमर, नित्य, शाश्वत और अजर-अमर है।
अन्य प्रासंगिक श्लोक :
“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।“
[ कठोपनिषद 1.3.14 ]
प्रसिद्ध कथन – “उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।” इसी वेदान्तिक आत्मविश्वास से प्रेरित है।
उत्तिष्ठत जाग्रत :
“उठो और जागो।” यह आह्वान है कि जीवन के उद्देश्यों के प्रति सचेत हो जाओ और आलस्य, अज्ञानता तथा मोह को त्यागकर अपनी चेतना को जाग्रत करो।
प्राप्य वरान्निबोधत :
“श्रेष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त करो और सत्य का ज्ञान प्राप्त करो।” यह जीवन के उच्चतम आदर्शों और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है।
- व्यावहारिक वेदान्त –
स्वामी विवेकानंद ने वेदान्त को केवल आध्यात्मिक चिंतन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे व्यावहारिक रूप से समाज में लागू करने की बात की।
प्रासंगिक श्लोक :
“” त्यजेत् कुर्वीत नीरस्यं तत् कर्म यन्न बन्धाय। “”
महाभारत, शांतिपर्व (12.35.8)
भावार्थ :
जो कार्य बंधन (संसार के मोह और कर्मों के जाल) का कारण बनता है, उसे त्याग देना चाहिए।
ऐसे कार्य करें जो बंधनरहित हों, अर्थात् जिनका फल व्यक्ति को आसक्ति में न बांधे।
अन्य प्रासंगिक श्लोक :
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।”
[ भगवद गीता 2.47 ]
विवेकानंद ने कर्म योग को भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत से जोड़ा। उन्होंने गीता के “निष्काम कर्म” के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने सिखाया कि बिना फल की इच्छा के कार्य करना ही सच्चा योग है।
विवेकानंद का दृष्टिकोण:
- आसक्ति मुक्त जीवन:
- हमारे कार्यों को इस प्रकार से करना चाहिए कि हम उनके परिणामों के प्रति आसक्त न हों।
- आज के जीवन में, हमें कर्म को धर्म और कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए।
- सुख और दुःख का विवेकपूर्ण चयन:
- हमें उन गतिविधियों को अपनाना चाहिए, जो न केवल हमारे लिए बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी सुखदायी हों।
- अपने व्यवहार में ऐसे कार्यों को त्याग देना चाहिए, जो दुःख या हानि का कारण बनते हैं।
उनकी “सेवा धर्म” की विचारधारा इस सिद्धांत पर आधारित थी।
- सार्वभौमिक एकता और भाईचारा –
विवेकानंद ने अद्वैत वेदान्त के सिद्धांत के माध्यम से विश्व-बंधुत्व और सार्वभौमिक एकता का संदेश दिया। उनका यह दृष्टिकोण शिकागो धर्म संसद के उनके ऐतिहासिक भाषण में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।
प्रासंगिक श्लोक :
एकोऽहम् बहुस्यामि।
छांदोग्य उपनिषद (6.2.3)
भावार्थ:
- एकोऽहम्: “मैं अकेला हूँ।”
- बहुस्यामि: “मैं अनेक हो जाऊँगा।”
“मैं एक हूँ और मैं अनेक रूपों में व्यक्त होना चाहता हूँ।”
विवेकानंद का दृष्टिकोण:
- ब्रह्म ही सृष्टि का मूल स्रोत है।
- सृष्टि की विविधता केवल उसकी लीला है।
- वास्तविकता में सब कुछ एक ही सत्य का विस्तार है।
अत: सभी धर्म, जातियां और संस्कृतियां एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं।
उनका मानना था कि धर्मों के बीच संघर्ष व्यर्थ है, क्योंकि हर धर्म का अंतिम लक्ष्य एक ही सत्य को प्राप्त करना है।
अन्य प्रासंगिक श्लोक :
“एकं सत विप्राः बहुधा वदन्ति”
[ ऋग्वेद 1.164.46 ]
सत्य (सत्य रूपी परमात्मा) एक ही है, परंतु ज्ञानी (विद्वान) लोग उसे अलग-अलग नामों और रूपों से पुकारते हैं।
इसी क्रम में –
“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।”
[ गीता 4.11 ]
“ जो मुझे जैसे भजते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार प्राप्त होता हूं। “
अन्य प्रासंगिक श्लोक :
“अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥”
[ पंचतंत्र, 5.3.37 ]
भावार्थ :
- लघुचेतसाम् : छोटे या संकीर्ण विचारों वाले लोग “यह मेरा है, और वह तुम्हारा है” जैसी बातें सोचते हैं।
- उदारचरितानाम् : जबकि उदार चरित्र वाले महान व्यक्तियों के लिए पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है।
भारतीय संस्कृति की उदार और समावेशी दृष्टि को दर्शाते हुये यह विचार “वसुधैव कुटुम्बकम्” के माध्यम से मानवता की एकता और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश देता है।
- लघुचेतस और उदारचरित:
- संकीर्ण मानसिकता :
- छोटे या स्वार्थी लोग हर चीज को “अपना” और “पराया” के दायरे में बांधकर देखते हैं।
- उनकी सोच सीमित होती है, और वे केवल अपने हितों तक सीमित रहते हैं।
- उदार मानसिकता :
- जिनका चरित्र महान और विचार विशाल हैं, उनके लिए सब समान हैं।
- उनके लिए न कोई पराया है और न कोई अपना। पूरी पृथ्वी उनका परिवार है।
- “वसुधैव कुटुम्बकम्” का संदर्भ:
- यह श्लोक भारतीय जीवन दर्शन की आधारशिला है।
- यह मानव मात्र के बीच कोई भेदभाव नहीं करता और सबको एक परिवार के रूप में देखता है।
स्वामी विवेकानंद ने भी इसी भावना का प्रचार किया और कहा कि –
- “सब मनुष्य एक ही ईश्वर के बच्चे हैं।”
- उनके अनुसार, जाति, धर्म, और राष्ट्रीयता से परे जाकर मानवता की सेवा करनी चाहिए।
- “वसुधैव कुटुम्बकम्” का संदेश हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही विश्व परिवार का हिस्सा हैं।
- इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों, वैश्विक शांति और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने में किया जा सकता है।
- स्वयं पर विश्वास और आत्मनिर्भरता –
वेदान्त के सिद्धांतों ने विवेकानंद को आत्मनिर्भरता और स्वयं पर विश्वास का उपदेश देने के लिए प्रेरित किया।
प्रासंगिक श्लोक:
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।
भगवद्गीता [ अध्याय 6.5 ]
भावार्थ :
- उद्धरेदात्मनात्मानं:
- “आत्मा द्वारा आत्मा का उद्धार करें।”
- मनुष्य को स्वयं अपने प्रयासों से अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए।
- नात्मानमवसादयेत्:
- “आत्मा को पतन की ओर न ले जाएं।”
- स्वयं को हानि, नकारात्मकता, या अधोगति में न धकेलें।
- आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः:
- “आत्मा स्वयं का मित्र है।”
- यदि व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तो वह अपना सबसे बड़ा मित्र बन जाता है।
- आत्मैव रिपुरात्मनः:
- “आत्मा स्वयं का शत्रु है।”
- यदि व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, तो वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है।
“मन ही मित्र है और मन ही शत्रु।”
विवेकानंद का दृष्टिकोण:
- स्वयं पर निर्भरता:
- किसी अन्य पर निर्भर रहने की बजाय, हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं पर विश्वास और प्रयास करना चाहिए।
- सकारात्मक सोच:
- मन को सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों से भरकर हम अपना मित्र बना सकते हैं।
- नकारात्मकता और आत्म-संदेह से बचना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी प्रगति को रोक सकते हैं।
- आत्म-विकास और आत्म-नियंत्रण:
- आज की व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में, आत्म-नियंत्रण (self-discipline) और आत्म-विकास (self-improvement) ही सफलता का मार्ग है।
- आत्म-विकास का मार्ग आत्म-नियंत्रण और आत्म-जागरूकता से होकर जाता है।
अंत में सारगर्भित संदेश वर्तमान परिपेक्ष्य में –
स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व आज के युग में भी असीम प्रासंगिकता रखता है। उनका जीवन हमें आत्म-निर्भरता, आत्म-जागृति और मानवता के प्रति समर्पण का संदेश देता है। वर्तमान समय में, जब दुनिया भौतिकवाद, असहिष्णुता और सामाजिक असमानताओं की चुनौतियों का सामना कर रही है, विवेकानंद के विचार एक मार्गदर्शक प्रकाशस्तंभ के समान हैं। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व केवल अतीत की प्रेरणा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान है। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि आत्म-ज्ञान, कर्मठता और मानवता की सेवा के माध्यम से व्यक्ति न केवल स्वयं को, बल्कि समाज और दुनिया को भी बेहतर बना सकता है। आज, जब आत्म-केंद्रितता और भौतिकता का बोलबाला है, स्वामी विवेकानंद का संदेश मानवता को एक नई दिशा देने की शक्ति रखता है।
आधुनिक संदर्भ में विवेकानंद के व्यक्तित्व का महत्व :-
- युवाशक्ति हेतु प्रेरणास्रोत –
“उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।”
“खुद पर विश्वास करो”
ये संदेश आज भी युवाओं को उनकी ऊर्जा और क्षमताओं को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं।
- धार्मिक सहिष्णुता और वैश्विक बंधुत्व का संदेश –
“वसुधैव कुटुम्बकम्” और धर्मों की सहिष्णुता का उनका सिद्धांत आज की दुनिया में शांति और सह-अस्तित्व के लिए एक आदर्श है।
- समानता और समावेशिता का संदेश –
जाति, धर्म, और वर्ग की बाधाओं को तोड़ते हुए “नर सेवा नारायण सेवा” का संदेश दिया। यह विचार आज के समाज में समरसता और समानता की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है।
- आध्यात्मिकता और आधुनिकता में सामंजस्य रखने को बल –
विवेकानंद ने दिखाया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। यह संतुलन आज की तकनीकी और तेजी से बदलती दुनिया में मानसिक शांति बनाए रखने का मार्ग है।
“” स्वामी विवेकानंद एक असीम शख्सियत थे जिनके बारे में संक्षिप्त में एक पंक्ति कहूँ तो –
“” भारतीय आध्यात्म, संस्कृति और वेदान्त दर्शन की आत्मा को दर्शन करवाती विचारशक्ति का दूसरा नाम स्वामी विवेकानन्द है। “”
These valuable are views on Swami Vivekanand Philosophical Thought | My view’s Swami Vivekanand | Swami Vivekanand
स्वामी विवेकानंद व्यक्तित्व पर एक संक्षिप्त लेखनी | स्वामी विवेकानंद एक दार्शनिक की नजर से
विचारानुगामी एवं प्रशंसक –मानस जिले सिंह
【यथार्थवादी विचारक】
अनुयायी – मानस पंथ
शिष्य – डॉ औतार लाल मीणा
विद्यार्थी – शोधार्थी, दर्शनशास्त्र विभाग 【 JNVU, Jodhpur 】
उद्देश्य – मानवीय मूल्यों को जगत के केंद्र में रखते हुऐ शिक्षा, समानता व स्वावलंबन का प्रचार प्रसार में अपना योगदान देने का प्रयास।
बेबसाइट- www.realisticthinker.com

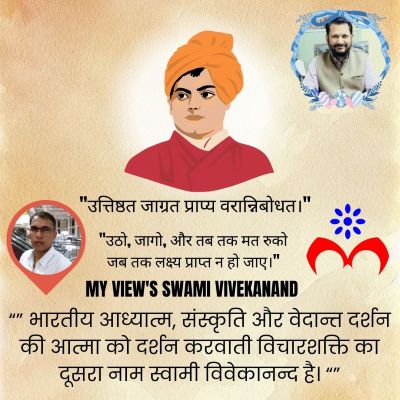

वास्तव मे इस लेख में अमूल्य विचारों से अवगत करवाया है जो कि आज के समय की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय युवा दिवस🙏
स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायी विचारों का
आज के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन करने वाला लेखन
अतिसुन्दर 👌👌
Bahut uttam ki likha hai aapne sir
बहुत ही सुंदर भाईसाहब। आपके द्वारा उक्त लेख में चयन किए गए शब्दों के आधार पर आप एक गहन चिंतनशील व बुद्धिमान व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। लेख का स्तर बहुत उच्च व गूढ़ है जो सामान्य विद्यार्थी या व्यक्ति की समझ से परे हो सकता है ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। अतः इस संबंध में मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि लेख का स्तर सामान्य रखा जाए तो अधिक समझ व पठनीय रहेगा। दूसरा सुझाव ये है कि आप लेख के शीर्षक में विवेकानंद जी के दर्शन या दार्शनिक आयाम, पहलू, देन जैसे शब्दों का चयन कर सकते हैं। (संदीप कुमार)
आदरणीय भाई साहब,
धन्यवाद |
Deep & value able knowledge of indian new generation